सुख का मापदण्ड और भारतीय यथार्थ
विश्व हैपीनेस रिपोर्ट की सीमाएँ और भारत में सहानुभूति–ढाँचे की अनिवार्यता
विश्व हैपीनेस रिपोर्ट में भारत की निम्न रैंकिंग अक्सर वास्तविक कल्याण स्थिति से अधिक सांस्कृतिक तथा धारणा-आधारित पूर्वाग्रहों को दर्शाती है। सुख मापने की पद्धति में निहित सीमाओं को समझते हुए भारत को अपने सामाजिक, संवेदनात्मक और सामुदायिक ढाँचे में सहानुभूति-आधारित सुधारों को बढ़ाना चाहिए।
— डॉ. सत्यवान सौरभ
विश्व हैपीनेस रिपोर्ट हर वर्ष किसी देश की सुख-संतुष्टि का आकलन प्रस्तुत करती है। किंतु भारत जैसे विशाल, विविध और सांस्कृतिक रूप से जटिल देश के लिए यह रिपोर्ट कई बार उस यथार्थ को उजागर नहीं कर पाती जो समाज के भीतर गहरे स्तर पर मौजूद है। भारत की रैंकिंग अक्सर सौ से ऊपर दिखाई देती है, जबकि इसी अवधि में भारत ने स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, संरचनात्मक सुधारों और गरीबी कमी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। यह विरोधाभास एक नैसर्गिक प्रश्न खड़ा करता है—क्या किसी देश के “सुख” को केवल सर्वेक्षण-आधारित दृष्टिकोण से समझा जा सकता है? और क्या यह मापन भारतीय जीवन-मूल्यों और सामाजिक वास्तविकताओं को पकड़ने में सक्षम है?
विश्व हैपीनेस रिपोर्ट का आधार मुख्यतः स्व-आकलन है। सर्वेक्षणकर्ता उत्तरदाताओं से पूछते हैं कि वे जीवन को दस-स्तरीय सीढ़ी में कहाँ रखते हैं। यह “सीढ़ी-संबंधी मूल्यांकन” पश्चिमी मनोविज्ञान में प्रयुक्त उस विचार पर आधारित है जिसमें सुख को व्यक्तिगत प्राप्तियों और परिस्थितियों के आधार पर मापा जाता है। परन्तु भारतीय समाज में सुख की अवधारणा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामुदायिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक आयामों से भी गहराई से जुड़ी होती है। भारतीय संस्कृति में संतोष, कर्तव्य, परस्पर सहायता, संबंधों की स्थिरता और आध्यात्मिक संतुलन भी सुख का महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। इसलिए जब एक भारतीय उत्तरदाता से पूछा जाता है कि वह दस में से अपने जीवन को कितने अंक देगा, तो उसके भीतर कई सांस्कृतिक कारक सक्रिय होते हैं—विनम्रता, शांत-स्वीकृति, परिस्थिति को भाग्य-नियति से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति, या समाज में शिकायत दिखाने से बचना। इसके परिणामस्वरूप अनेक भारतीय अपने जीवन को कम अंक दे सकते हैं, भले ही वे वस्तुतः अनेक स्तरों पर बेहतर स्थिति में हों।
सर्वेक्षण का नमूना आकार भी भारत के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले, शहरी और ग्रामीण विविधताओं से भरे देश के लिए मात्र लगभग एक हज़ार लोगों के उत्तर पर आधारित निष्कर्ष असंतुलित हो सकते हैं। भारतीय समाज क्षेत्रीय, भाषायी, आर्थिक तथा सामाजिक स्तरों पर अत्यंत विषम है; एक छोटे नमूने का उपयोग करके उस विविधता का प्रतिनिधित्व संभव नहीं। एक जिले के ग्रामीण किसान की जीवन-संतुष्टि की अवधारणा दिल्ली के शहरी पेशेवर व्यक्ति से भिन्न हो सकती है। फिर भी, दोनों को समान पैमाने पर रखकर किसी राष्ट्रीय “सुख-अंक” की व्याख्या करना वैज्ञानिक रूप से सीमित प्रतीत होता है।
इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में प्रयुक्त सुख की अवधारणा भी सांस्कृतिक पक्षपात से प्रभावित है। पश्चिमी ढाँचा सुख को भौतिक उपलब्धियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रत्यक्ष संतुष्टि से जोड़ता है, जबकि भारतीय समाज में अनेक बार सुख का अर्थ कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाए रखना, भावनात्मक सहारा, सामुदायिक सहयोग या आध्यात्मिक शांति से भी जुड़ा होता है। यह अंतर सर्वेक्षणकर्ता की भाषा, शैली, शब्दों और उत्तरदाता के मनोभाव को प्रभावित करता है। अक्सर यह देखा गया है कि भारत के ग्रामीण या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में उत्तरदाता “जीवन के अंक” को किसी ऐसे प्रश्न की तरह स्वीकार करते हैं जिसमें शिकायत या असंतोष दिखाना उचित नहीं लगता। इसी वजह से कई भारतीय वास्तविक अनुभव होने के बावजूद संतुष्टि को अपेक्षाकृत कम आंकते हैं, जिससे परिणाम और अधिक विकृत होते हैं।
इसके विपरीत, भारत ने बीते वर्षों में सामाजिक कल्याण में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। करोड़ों लोगों तक निःशुल्क खाद्यान्न पहुँचाना, सर्वजन स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों में विस्तार, शिक्षा तथा महिला-शिशु पोषण कार्यक्रमों में बढोत्तरी—ये सब समग्र जीवन-गुणवत्ता को बढ़ाने वाले उपाय रहे हैं। किन्तु अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें इन संकेतकों को केवल सीमित रूप से जोड़ती हैं, क्योंकि उनका मूल केंद्र “अनुभूत संतुष्टि” पर आधारित है, न कि “वस्तुनिष्ठ कल्याण” पर। यही कारण है कि वस्तुनिष्ठ रूप से बेहतर होती सुविधाएँ भी रिपोर्ट में पर्याप्त रूप से उजागर नहीं हो पातीं। भारत में गरीबी में कमी और स्वास्थ्य-सेवाओं की पहुँच में वृद्धि ने जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाया है, परन्तु सुख-सर्वेक्षण इस सकारात्मक परिवर्तन को मापने में अक्षम रहते हैं।
ऐसे में, प्रश्न यह उठता है कि भारत को अपने भीतर ऐसा क्या बदलना चाहिए जिससे समाज अधिक भावनात्मक रूप से सुरक्षित, सहानुभूतिपूर्ण और संतुलित बन सके। इसका उत्तर “सहानुभूति संरचना”—एक व्यापक सामाजिक ढाँचा है जिसमें राज्य, समाज, संस्थान और समुदाय मिलकर नागरिकों को भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक सहारा, संवाद और सहायता प्रदान करें। इस ढाँचे का पहला स्तंभ मानसिक-स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। भारत में मानसिक-स्वास्थ्य को लेकर अभी भी कई भ्रम और कलंक मौजूद हैं। लोग सहायता लेने में संकोच करते हैं, और प्राथमिक चिकित्सा ढाँचे में मानसिक स्वास्थ्य की अनुपस्थिति समस्या को बढ़ाती है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित परामर्शदाता हों, दूरभाष-आधारित सेवाएँ व्यापक हों और विद्यालयों-कॉलेजों में मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध हो, तो समाज में भावनात्मक असुरक्षा घट सकती है।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समुदाय-आधारित सहयोग है। भारतीय संस्कृति में पड़ोस, परिवार और सामाजिक संबंधों की शक्ति अत्यधिक रही है, परन्तु शहरीकरण और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के कारण यह संरचना कमजोर हो रही है। यदि स्थानीय समुदायों में संवाद-चक्र, सहारा-समूह, वरिष्ठ नागरिक सहायता-केंद्र, महिलाओं के लिए सुरक्षित समुदाय-स्थल और युवाओं के लिए साझा सहयोग मंच विकसित किए जाएँ, तो सामाजिक एकांत कम हो सकता है। सहानुभूति तभी विकसित होती है जब लोग एक-दूसरे के जीवन में उपस्थिति का अनुभव करें।
सहानुभूति संरचना का तीसरा स्तंभ कार्यस्थल है। कार्यस्थलों पर तनाव, प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य-दबाव और असुरक्षा बढ़ रही है, जिसके चलते कर्मचारियों का मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। यदि संस्थान संवेदनशील नीति अपनाएँ—कार्य अवधि में लचीलापन, परामर्श सेवाएँ, साथी-सहयोग कार्यक्रम, नेतृत्व प्रशिक्षण में सहानुभूति-आधारित व्यवहार—तो यह वातावरण को स्वस्थ बना सकता है। एक सहानुभूतिपूर्ण संस्थागत संस्कृति न केवल कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाती है बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाती है।
चौथा आयाम विद्यालयों में भावनात्मक शिक्षा का है। बच्चों में सहानुभूति, अहिंसक संवाद, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोगात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि बच्चे अपनी भावनाएँ समझना, व्यक्त करना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना सीखें, तो समाज भविष्य में अधिक संवेदनशील बनेगा। शैक्षणिक ढाँचा केवल परीक्षा-आधारित न रहकर जीवन-आधारित होना चाहिए।
पाँचवाँ पक्ष तकनीकी सहारा है। यदि तकनीक का उपयोग मानसिक-स्वास्थ्य और भावनात्मक सहयोग के लिए किया जाए—जैसे परामर्श ऐप, संकट में सहायता, छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल संवाद केंद्र—तो यह सहानुभूति संरचना को व्यापक बना सकता है। तकनीक का जिम्मेदार उपयोग सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकता है, बशर्ते उसकी निगरानी और नैतिकता मजबूत हो।
अंततः, राज्य के प्रशासनिक ढाँचे में भी सहानुभूति की आवश्यकता है। जब सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, परिवहन, सुरक्षा और न्याय-प्रणाली में कार्यरत लोग नागरिकों के प्रति अधिक करुणामय व्यवहार अपनाएँ, तो नागरिक-राज्य संबंध और भी मजबूत होते हैं। जनता की समस्याओं को सुनना, सम्मान देना और समाधान में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।
इस प्रकार विश्व हैपीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग उसे केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय एक अवसर के रूप में समझा जाना चाहिए। यह अवसर भारतीय समाज को यह विचार करने का मार्ग देता है कि कैसे हम “सुख” को केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक भरोसा, संवेदनशील संवाद और मानसिक-स्वास्थ्य संरचना के रूप में विकसित कर सकते हैं। रिपोर्ट की पद्धति में चाहे जितनी सीमाएँ हों, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज किस दिशा में जाए। भारत यदि अपनी पारंपरिक सामुदायिक शक्ति को आधुनिक सामाजिक-कल्याण ढाँचे के साथ जोड़ दे, तो सहानुभूति-आधारित विकास की एक नई धारा स्थापित हो सकती है, जो वास्तविक सुख को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।
— डॉ. सत्यवान सौरभ




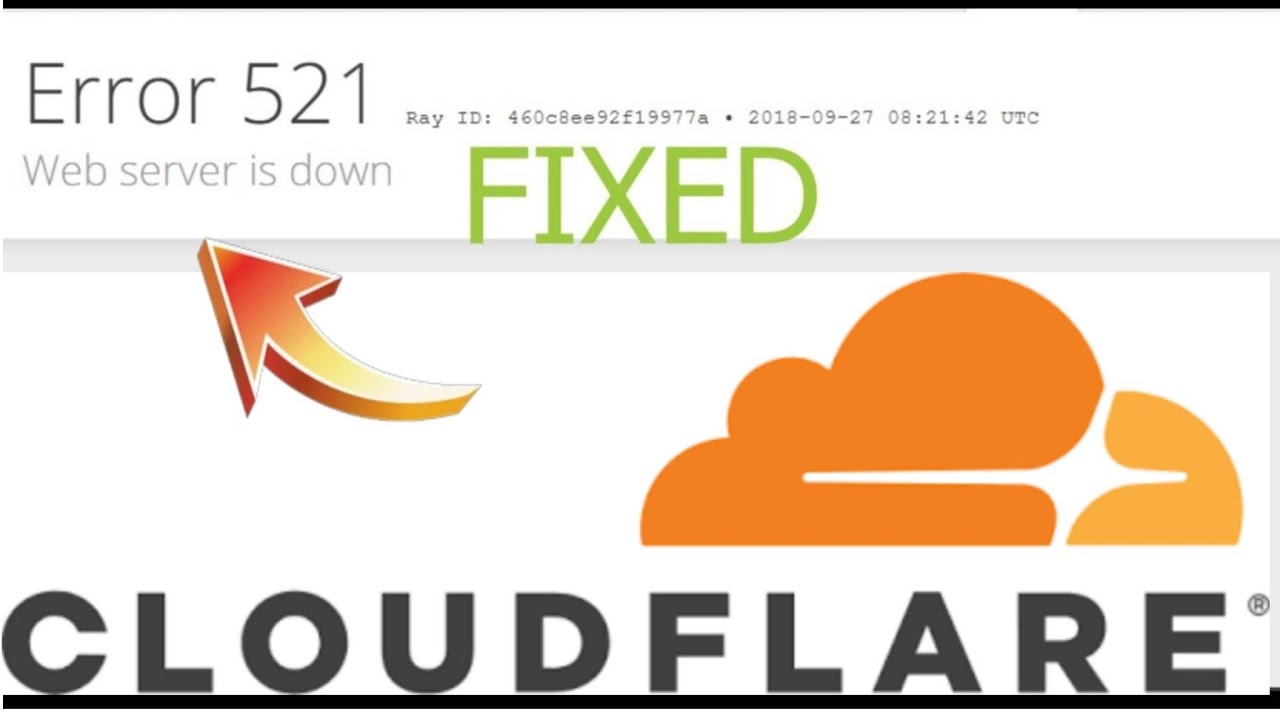
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!