शिक्षक नौकरी छोड़ रहे हैं – एक कड़वा सच
– क्योंकि शिक्षक को शिक्षण कार्य नहीं करवा कर एक बहुद्देशीय कर्मचारी बना दिया गया है। जब शिक्षक को शिक्षण कार्य छोड़कर काग़ज़ों, रिपोर्टों और आयोजनों का भार दे दिया जाता है, तो शिक्षा अपनी आत्मा खो देती है।
देश की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ सबसे बुनियादी स्तंभ — शिक्षक — स्वयं डगमगाने लगा है।
कभी यह पेशा समाज में सम्मान, स्थिरता और प्रेरणा का प्रतीक था, पर आज वही शिक्षक काग़ज़ी औपचारिकताओं, तकनीकी दबाव और प्रशासनिक आदेशों के बीच खो गया है।
वह थक चुका है, निराश है, और अनेक शिक्षक अब यह पेशा छोड़ रहे हैं। यह कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतावनी है — क्योंकि जब शिक्षक थक जाता है, तब शिक्षा मर जाती है।
आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहाँ शिक्षक सबसे असहाय और अवमूल्यित स्थिति में पहुँच चुका है। कभी यह पेशा सम्मान, आदर्श और आत्मसंतोष का प्रतीक हुआ करता था। शिक्षक वह व्यक्ति था जो समाज की दिशा तय करता था, बच्चों के भीतर मूल्य और विवेक का बीजारोपण करता था। पर अब स्थिति यह है कि शिक्षण सेवा धीरे-धीरे एक प्रशासनिक बोझ में तब्दील हो गई है। शिक्षक का समय अब बच्चों से अधिक कागज़ों, रिपोर्टों और ऑनलाइन पोर्टलों पर बीतने लगा है। हर दिन नई योजना, नया निर्देश, नया ऐप और नए फॉर्म की मांग। शिक्षण अब नौकरी बन गया है, और नौकरी इतनी जटिल कि उसमें पढ़ाने का समय ही नहीं बचा। जब हर कार्य का प्रमाण मांगने वाला सिस्टम बन जाता है, तो भरोसा और रचनात्मकता दोनों समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि आज एक बड़ा वर्ग शिक्षक होने के बावजूद शिक्षण से कट गया है — और जो नई पीढ़ी है, वह अब इस पेशे को अपनाने में रुचि नहीं दिखा रही। वह देख रही है कि यह पेशा अब प्रेरणा नहीं, थकान और तनाव का प्रतीक बन चुका है।
तकनीक और प्रशासनिक निगरानी के नाम पर शिक्षा को जिस दिशा में धकेला जा रहा है, उसने शिक्षक को डेटा-कलेक्टर और इवेंट मैनेजर बना दिया है। हर महीने किसी न किसी दिवस का आयोजन — योग दिवस, मातृभाषा दिवस, साक्षरता दिवस — और हर आयोजन का फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, लिंक… यह सब दिखावे की संस्कृति में बदल गया है। विद्यालय अब ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि प्रदर्शन का मंच बन गए हैं। शिक्षक बच्चों को कम और कैमरे को ज़्यादा संबोधित करता दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बोझ और भी भारी है। दो या तीन शिक्षक सैकड़ों बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं। मिड-डे मील, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म, साइकिल वितरण, सर्वे, जनगणना — सब कुछ उसी के सिर पर। शिक्षा धीरे-धीरे प्रबंधन बन गई है, और शिक्षक एक सरकारी कर्मचारी जो सबका आदेश माने। इस स्थिति ने न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, बल्कि शिक्षक के भीतर की सृजनात्मकता और आत्मसम्मान को भी क्षीण कर दिया है।
इन परिस्थितियों का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षक की मानसिक स्थिति पर पड़ा है। निरंतर निगरानी, आंकड़ों की मांग, और हर कार्य का डिजिटल प्रमाण — इन सबने शिक्षा को मानवीयता से दूर कर दिया है। जो शिक्षक कभी अपने विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक रिश्ता रखते थे, वे अब एक यंत्रवत भूमिका निभाने को विवश हैं। उनके पास न समय है, न अवसर कि वे किसी बच्चे की समस्या को समझ सकें, उसे प्रेरित कर सकें या उसके साथ संवाद कर सकें। परिणामस्वरूप, शिक्षक भावनात्मक रूप से थक रहे हैं, और विद्यार्थी भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। छात्र अब शिक्षक को मार्गदर्शक नहीं, सेवा प्रदाता मानने लगे हैं। यह दृष्टिकोण शिक्षा की आत्मा को भीतर से तोड़ रहा है। सम्मान और भरोसे का जो रिश्ता कभी शिक्षा की नींव था, वह अब संदेह और औपचारिकता के बोझ तले दब गया है।
यह स्थिति केवल शिक्षकों की नहीं, बल्कि समाज के भविष्य की चिंता है। यदि शिक्षा का केंद्र शिक्षक और विद्यार्थी नहीं रहेंगे, तो विद्यालय केवल भवन बनकर रह जाएंगे। योजनाएँ, पोर्टल, और नीतियाँ तभी सार्थक हैं जब वे मानवीय जुड़ाव को बढ़ाएँ, न कि खत्म करें। हमें इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचना होगा — क्या हम अपने शिक्षकों पर भरोसा करते हैं? क्या हम उन्हें वह स्वतंत्रता और सम्मान दे रहे हैं जिसकी शिक्षा को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? जब शिक्षक को केवल आदेश पालन करने वाला कर्मचारी बना दिया जाता है, तो वह प्रेरक नहीं रह जाता। और जब प्रेरणा खत्म होती है, तो शिक्षा का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षक ही वह केंद्र है जिसके इर्द-गिर्द पूरी शिक्षा व्यवस्था घूमती है। यदि वह निराश, उपेक्षित और थका हुआ है, तो आने वाली पीढ़ी भी वैसी ही बनेगी। अब समय है शिक्षक को दोबारा शिक्षा के केंद्र में लाने का — क्योंकि यदि शिक्षक चला गया, तो विद्यालय तो रह जाएगा, पर शिक्षा नहीं।
यह केवल शिक्षकों की समस्या नहीं, बल्कि समाज के भविष्य की चुनौती है। यदि शिक्षा से उसका आत्मीय तत्व — शिक्षक — कमजोर पड़ गया, तो आने वाली पीढ़ी का बौद्धिक और नैतिक विकास भी अधूरा रह जाएगा। नीतियाँ, योजनाएँ, ऐप और पोर्टल तभी उपयोगी हैं जब वे शिक्षक को सशक्त बनाएँ, न कि उसे बोझिल करें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षा का केंद्र शिक्षक और विद्यार्थी ही हैं — ना कि आंकड़े, फाइलें और फ़ोटो। शिक्षक को फिर से स्वतंत्रता, सम्मान और भरोसे का वातावरण देना होगा। वह केवल नौकरी नहीं कर रहा, वह भविष्य गढ़ रहा है। यदि उसे प्रेरणा और गरिमा नहीं मिली,
तो शिक्षा केवल भवनों और आंकड़ों में सीमित रह जाएगी।
हमें यह याद रखना चाहिए — जब शिक्षक चला जाएगा, विद्यालय तो रह जाएगा, पर शिक्षा नहीं।
– डॉ. प्रियंका सौरभ

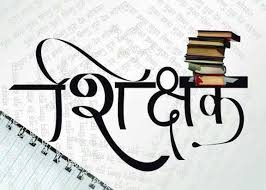


Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!