हिंदी दिवस का संदेश: मातृभाषा में शिक्षा ही वास्तविक प्रगति
(भाषा से जुड़ता है समाज और संस्कृति मातृभाषा में शिक्षा ही वास्तविक राष्ट्रनिर्माण का मार्ग)
मातृभाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति से जुड़ाव का माध्यम है। नई शिक्षा नीति (2020) ने कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया है, जिससे बच्चों की समझ, आत्मविश्वास और भागीदारी बढ़ेगी। अंग्रेज़ी का महत्व अपनी जगह है, परंतु प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही सबसे प्रभावी है। चुनौतियों के बावजूद मातृभाषा आधारित शिक्षा से ड्रॉपआउट दर घटेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी और बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। हिंदी दिवस हमें यही संदेश देता है कि मातृभाषा ही सच्ची शिक्षा और राष्ट्रनिर्माण का आधार है।
– डॉ. सत्यवान सौरभ
भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, संस्कृति और समाज से जुड़ने का आधार है। जिस भाषा में हम सोचते, सपने देखते और अभिव्यक्त होते हैं, वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में मातृभाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और गर्व का भाव पैदा करना है। हिंदी दिवस केवल हिंदी के प्रचार-प्रसार का अवसर नहीं है, बल्कि यह मातृभाषाओं के महत्व और शिक्षा में उनके उपयोग पर विचार करने का भी अवसर है।
मातृभाषा व्यक्ति की सोच, संस्कार और भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती है। यह बच्चों के लिए सीखने का सबसे स्वाभाविक और सहज माध्यम है। जब कोई बच्चा अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो वह अधिक आत्मविश्वास और रुचि से सीखता है। मातृभाषा बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करती है, यह उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ती है, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाला छात्र बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाता है और यह शिक्षा को रटने की बजाय समझने की प्रक्रिया बनाती है।
भारत सरकार ने 34 वर्षों बाद 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। इस नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे अहम निर्णय था कि कक्षा 5 तक और जहां संभव हो वहां 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा उसी भाषा में मिलेगी जिसमें वे घर और समाज में बातचीत करते हैं। अनुसंधानों से भी यह सिद्ध हुआ है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा मिलने से बच्चे की समझ बेहतर होती है, ड्रॉपआउट दर कम होती है और कक्षा में उनकी भागीदारी अधिक होती है।
भारतीय संविधान भी मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन करता है। अनुच्छेद 350A कहता है कि राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कोठारी आयोग (1964-66) ने सुझाव दिया था कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा स्थानीय जनजातीय भाषा में होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) में भी यह प्रावधान किया गया कि जहां तक संभव हो, शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो।
आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभिभावक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में माता-पिता बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजने की होड़ में लगे रहते हैं। वे मानते हैं कि अंग्रेजी ही सफलता की कुंजी है। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना केवल “अंग्रेजी” को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीण भारत में निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में दाखिले की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाषा कभी भी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। असली सफलता अच्छी शिक्षा, आत्मविश्वास और ज्ञान पर आधारित होती है। यदि बच्चे को ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाए जिसे वह समझ ही नहीं पाता, तो न तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और न ही वह शिक्षा का सही लाभ ले पाएगा।

मातृभाषा में शिक्षा देने के अनेक लाभ हैं। बच्चा उसी भाषा में आसानी से सोच सकता है जो उसकी मातृभाषा है। अपनी भाषा में सीखने से भयमुक्त वातावरण मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चा अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा रहता है। जब शिक्षा सरल और बोधगम्य होगी तो बच्चे स्कूल छोड़ेंगे नहीं। मातृभाषा में सोचने और व्यक्त करने से सृजनात्मक क्षमता भी विकसित होती है।
लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने में कई व्यावहारिक समस्याएँ सामने आती हैं। भारत में भाषाओं और बोलियों की बहुत अधिक विविधता है। कई भाषाओं के पास मानकीकृत लिपि या पर्याप्त शिक्षण सामग्री नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, जो बहुभाषी कक्षाओं को संभाल सकें। नई पुस्तकों और प्रशिक्षण पर अतिरिक्त खर्च आएगा। साथ ही, अभिभावकों की मानसिकता भी एक बड़ी चुनौती है जो अंग्रेजी को ही श्रेष्ठ मानती है।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बहुभाषी शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ। मातृभाषाओं में गुणवत्तापूर्ण किताबें तैयार की जाएँ। अभिभावकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएँ ताकि वे समझें कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के लिए अधिक लाभकारी है। विभिन्न राज्यों में मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रयोग किए जाएँ और उनकी सफलता के आधार पर आगे बढ़ा जाए। डिजिटल शिक्षा सामग्री को भी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए।
दुनिया के कई देशों में मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती है और वहां प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर ही जोर दिया जाता है। जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी भाषा में शिक्षा देकर विश्व स्तर पर आर्थिक और तकनीकी प्रगति हासिल की। यूनैस्को भी लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए।
हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि अपनी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान का आधार है। यदि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी आत्मविश्वासी, ज्ञानवान और रचनात्मक बने तो हमें शिक्षा में मातृभाषा का स्थान सुनिश्चित करना होगा। हिंदी सहित सभी मातृभाषाओं का सम्मान करना आवश्यक है।
मातृभाषा में शिक्षा देने का विचार कोई नया नहीं है, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने की ज़रूरत है। अंग्रेजी का महत्व अपनी जगह है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही सबसे प्रभावी सिद्ध हो सकती है। हमें यह धारणा तोड़नी होगी कि केवल अंग्रेजी माध्यम से ही सफलता मिलती है। सफलता का असली आधार है— ज्ञान, समझ और आत्मविश्वास।
इस हिंदी दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी भाषा और संस्कृति के महत्व को पहचानेंगे, अभिभावकों को जागरूक करेंगे और बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यही वास्तविक राष्ट्र निर्माण की दिशा में हमारा योगदान होगा।
– डॉ. सत्यवान सौरभ




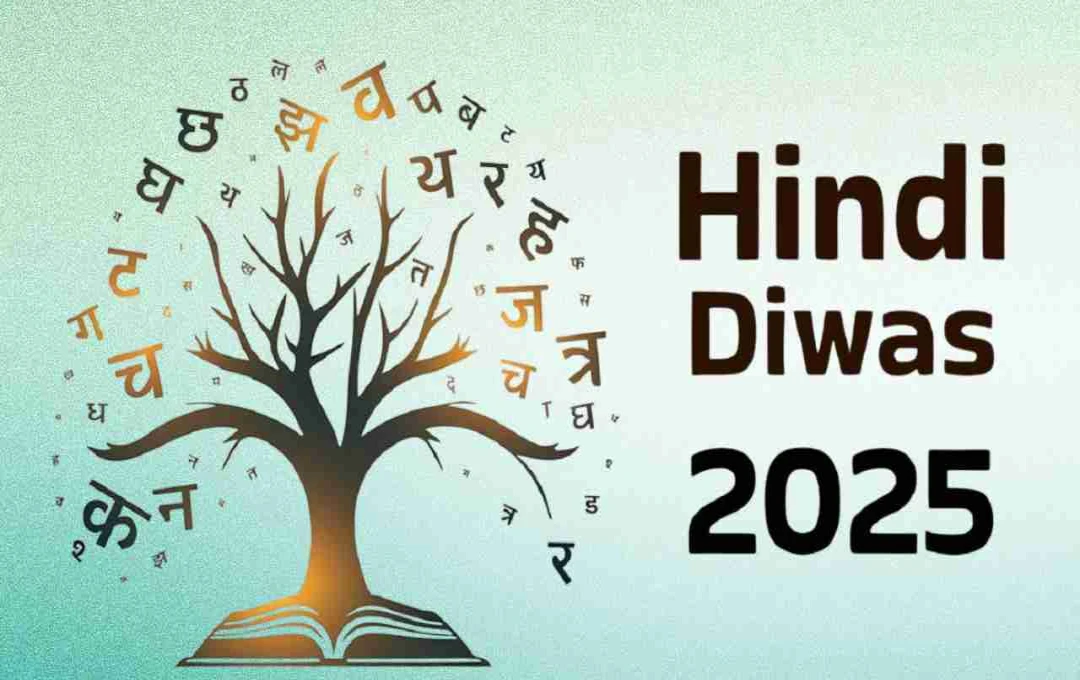
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!