भारत में 10.6 प्रतिशत वयस्क मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित !
आज पूरी दुनिया मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रही है। आपा-धापी व भागम-भाग भरी इस जिंदगी में हर कोई व्यक्ति कहीं न कहीं तनाव, अवसाद झेल रहा है।कहना ग़लत नहीं होगा कि सामाजिक दबाव, डिजिटल निर्भरता और आर्थिक असुरक्षा ने मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित किया है। युद्ध, प्रवासन और प्राकृतिक आपदाएँ भी कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य संकट का कारण हैं। वैश्विक परिदृश्य की यदि हम यहां पर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, हर 8 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। इस आलेख में ऊपर जानकारी दे चुका हूं कि अवसाद (डिप्रेशन) और चिंता ( एंक्साइटी) सबसे सामान्य समस्याएँ हैं, जो कामकाजी क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। आत्महत्या (सुसाइड) 15-29 वर्ष आयु वर्ग में प्रमुख मृत्यु कारणों में से एक है।जब कोविड-19 महामारी आई तो इसने अकेलेपन, तनाव और अवसाद को और बढ़ा दिया।
बहरहाल,दुनियाभर में एक अरब लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। दरअसल, इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने नई रिपोर्ट जारी की है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में चिंता और अवसाद को सबसे आम बताया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन बीमारियों की वजह से इंसान के जीवन और सेहत के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। वर्ष 2021 में 7.27 लाख लोगों ने अवसाद के कारण आत्महत्या की। वहीं डिप्रेशन और चिंता से हर साल अर्थव्यवस्था को लगभग एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ कामकाजी क्षमता घटने से हो रहा है। यदि हम यहां पर भारत में स्थिति की बात करें तो निम्हांस (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 10.6 प्रतिशत वयस्क मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। यहां मानसिक स्वास्थ्य विकारों का जीवनकाल प्रसार 13.7% है। वहीं मानसिक विकारों से ग्रस्त 70 से 92 प्रतिशत लोगों को अच्छा उपचार नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अवसाद से पीड़ित महिलाएं स्वास्थ्य देखभाल पर तीन गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं।
करीब आठ हजार से अधिक महिलाओं के डाटा का विश्लेषण किया गया। पाया गया 24 से 44 वर्ष की महिलाएं औसतन तीन से पांच हजार रुपये स्वास्थ्य पर खर्च कर रही हैं, जो उनकी आर्थिक आय से अधिक है। इसमें यह भी देखा गया कि करीब 71 फीसदी महिलाओं में चिंता और अवसाद दोनों मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। रिपोर्ट में सकारात्मक बदलाव की बात भी कही गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 71 फीसदी देशों ने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल करना शुरू कर दिया है। वहीं आपातकालीन हालात में मानसिक सहायता देने की क्षमता तेजी से बढ़ी है। 2020 में यह सुविधा 39 देशों में थी, जो अब बढ़कर 80 फीसदी से अधिक हो गई है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य संकट की समस्या आज एक बड़ी व गंभीर समस्या बन चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज की तेज़-रफ़्तार और प्रतिस्पर्धी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य संकट वैश्विक स्तर पर गंभीर समस्या बन चुका है और यह संकट केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से हर वर्ष लगभग 26 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं।वास्तव में इस मानसिक स्वास्थ्य संकट के प्रमुख कारणों की यदि हम यहां पर बात करें तो इनमें क्रमशः तेज़ जीवनशैली और प्रतिस्पर्धा, तनाव, नौकरी का दबाव और आर्थिक असुरक्षा, सोशल मीडिया और डिजिटल लत, पारिवारिक /सामाजिक टूटन और अकेलापन तथा युद्ध, प्रवासन, प्राकृतिक आपदाएँ आदि को शामिल किया जा सकता है।
मानसिक स्वास्थ्य संकट के प्रभाव स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था पर लगातार पड़ रहे हैं। यदि हम यहां पर स्वास्थ्य पर प्रभावों की बात करें तो इससे नींद की समस्या, नशे की लत, शारीरिक रोगों का खतरा बढ़ना, समाज पर प्रभावों की बात करें तो इससे रिश्तों में दरार, अपराध और हिंसा में बढ़ोतरी तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की यदि हम यहां पर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान सिर्फ उत्पादकता घटने के कारण होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्व देकर व इस संबंध में जागरूकता अपनाकर मानसिक स्वास्थ्य संकट का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और काउंसलिंग को प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे का हिस्सा बनाने की दिशा में काम करें। समुदाय और परिवार की भूमिका की बात करें तो सहानुभूति और समर्थन देकर इस समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। व्यक्तिगत प्रयास जैसे कि ध्यान, योग, व्यायाम, डिजिटल डिटॉक्स, और ज़रूरत पड़ने पर थेरेपी आदि लेना,इस दिशा में मददगार कदम साबित हो सकते हैं। इसके अलावा, कार्यस्थल पहल जैसे कि कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और लचीलापन अन्य कदम हैं। वास्तव में, आज दुनिया को मानसिक स्वास्थ्य को ‘विकल्प’ नहीं बल्कि प्राथमिकता बनाना होगा। आज मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों और कलंक को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने, स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।
इतना ही नहीं, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान भी इस क्रम में काफी मददगार साबित हो सकते हैं।ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-मेडिसिन और ऑनलाइन काउंसलिंग को बढ़ावा देने के साथ ही साथ आज जरूरत इस बात की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्तियां भी की जाएं। इसके साथ ही, सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त या कम खर्च पर उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए। नीतिगत सुधारों की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य नीति और मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 का बेहतर क्रियान्वयन आज की महत्ती आवश्यकता है।मानसिक स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके साथ ही कार्यस्थलों पर एम्प्लोई असिस्टेंस प्रोग्राम्स(ईएपी) लागू करने की जरूरत है, ताकि नौकरी से जुड़े तनाव को कम किया जा सके। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य ऐप्स और हेल्पलाइन (जैसे किरण हेल्पलाइन) का प्रचार किया जाना चाहिए तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ)आधारित चैटबॉट और काउंसलिंग सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
छात्रों के लिए परीक्षा तनाव और करियर दबाव को कम करने हेतु परामर्श सेवाएँ, किसानों और श्रमिक वर्ग में आत्महत्या रोकथाम के लिए आर्थिक व मानसिक समर्थन तथा महिलाओं, और बुजुर्गों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करके कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स तैयार करने चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में तनाव प्रबंधन और माइंडफुलनेस कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है।कुल मिलाकर, यह बात कही जा सकती है कि आज हमारे देश भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट हल करने के लिए केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि जागरूकता, शिक्षा, नीति सुधार, समाज की सोच और तकनीक—सभी को मिलाकर एक व्यापक रणनीति अपनानी होगी। तभी वास्तव में हम इस समस्या से निजात पा सकेंगे और हमारे देश को एक खुशहाल, समृद्ध व विकसित राष्ट्र बना सकेंगे। हमारे छोटे-छोटे प्रयासों और पहल से बहुत कुछ संभव हो सकता है।

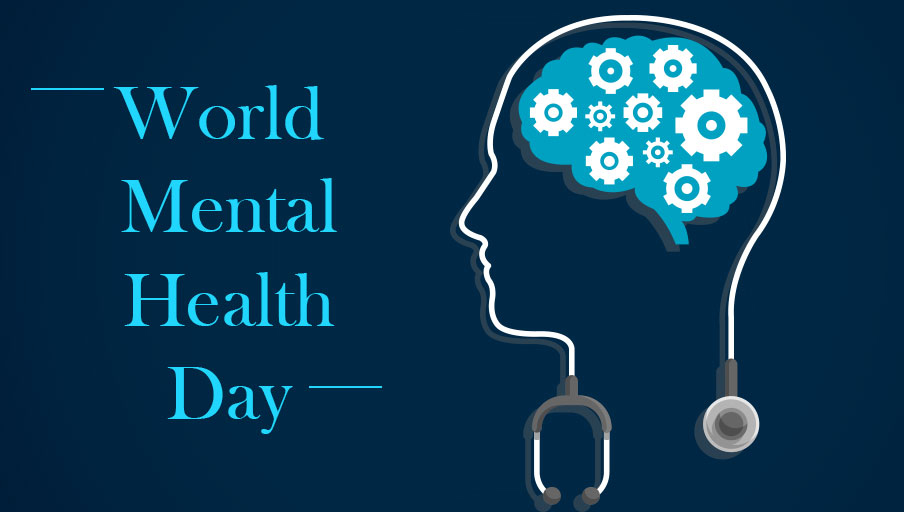


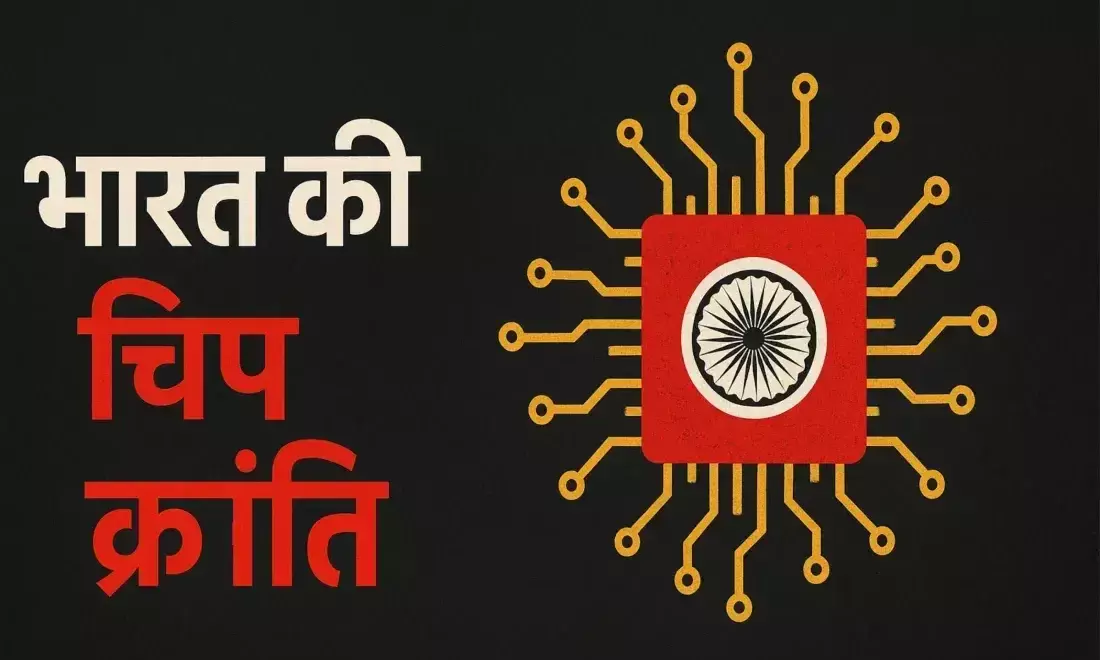
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!